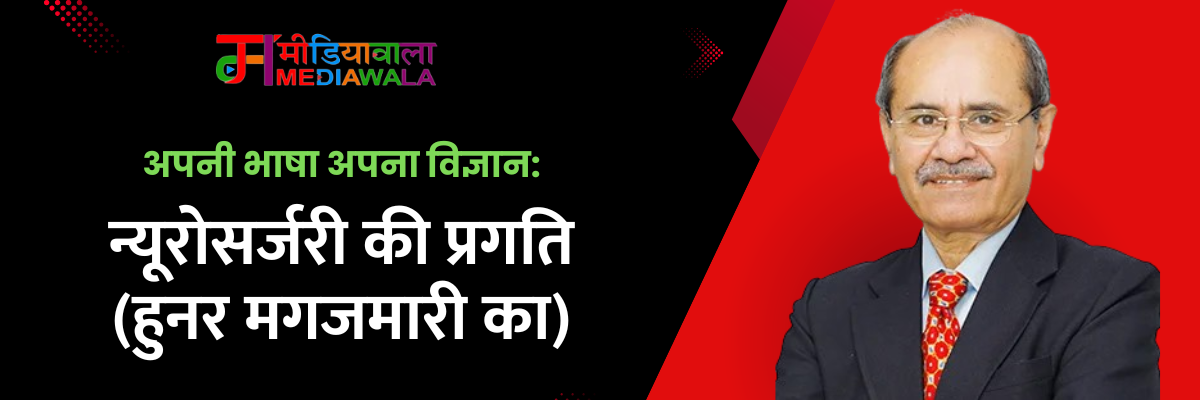डॉ. पौराणिक:- हिंदी साहित्य के लगभग पिछली एक आधी शताब्दी के इतिहास में मूर्धन्य नाम श्री कमलेश्वर।
हिंदी की कथा परंपरा के अग्रणी हस्ताक्षर, श्री कमलेश्वर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रचनात्मक हस्तक्षेप रखते हैं जिन्होंने अपने नेतृत्व में और अपने लेखनी से हिंदी साहित्य में दलित और समांतर परंपराओं को बढ़ावा दिया।
ऐसे मूर्धन्य अग्रणी साहित्यकार आदरणीय श्री कमलेश्वर जी। आज हमारे बीच इंदौर दूरदर्शन के स्टूडियो में उपस्थित हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार!
डॉ. पौराणिक:- कमलेश्वर जी
कमलेश्वरजी:- जी
डॉ पौराणिक:- आपने अपने लेखन का आरंभ जब किया तो शुरू में आपकी पहचान एक छोटे कस्बों से आने वाले कथाकार, साहित्यकार के रूप में थी और आपने वहां की संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। थोड़ा सा उस पृष्ठभूमि तक जाते हुए क्या आप बाद के अपने विकास और अवदान पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहेंगे?
कमलेश्वरजी:- डॉक्टर साहब! ऐसा है कि कस्बों की जब बात आती है और कस्बे के लेखन की तो उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमारे समय का आजादी के तत्काल बाद का एक तो विभाजन तो विस्थापन इतना हुआ था लोगों का चाहे सरहद पर से हुआ हो
डॉ पौराणिक:- या अंदर हुआ या
कमलेश्वरजी:- अंदर हुआ हो खासतौर से इसलिए, कि आजादी के तत्काल बाद गांव से ग्रामों से हमारी जो कृषि संस्कृति है उसके गांव से जो यदि विस्थापन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन निष्क्रमण जी वो निष्क्रमण जब हुआ तो बहुत से लोग तो शहरों तक पहुंच पाए बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए तो वो कहीं ना कहीं कस्बों में रुके तो ये एक तरह की सराय थी उनके लिए कुछ लोग जो शहर में हार जाते थे या शहर से परेशान हो जाते थे वो कस्बे में लौट आते थे कुछ जो आगे जाने वाले थे वो कस्बे में रुक के आगे बढ़ते थे तो मुझे लगता था कि एक बहुत ही बड़े संक्रमण का दौर था ये।
डॉ पौराणिक:- जी।
कमलेश्वरजी:- उस समय जो एक यथार्थ था और इसलिए मुझे लगा कि निश्चित रूप से वहां के यथार्थ को अगर पकड़ा जाए तो बेहतर होगा और वह यथार्थ आगे बढ़ते बढ़ते फिर निश्चित रूप से मुझे लगा कि एक बड़े भारी फलक पर एक इतने बड़े फलक पर जिसमें कि लगा ये कि समता समानता और न्याय की दुनिया जी का जो एक सवाल उठा था और उसमें खास तौर से जिस तरह से मराठी का दलित लेखन सामने आया था तो उस समय मुझे लगा था कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह भी एक तरह का मानसिक और एक तरह का आत्मिक संक्रमण है
डॉ पौराणिक:- जी।
कमलेश्वरजी:- जो यह चाह रहे हैं और यह इनका चाहना बड़ा उचित भी था और चाहना उचित क्या है इसमें किसी के देने का सवाल नहीं है इस न्याय के व अधिकारी थे
डॉ पौराणिक:– अधिकारी थे।
कमलेश्वरजी:- हे ना तो ऐसी स्थिति में मुझे यह लगा कि चाहे वह दलित साहित्य हो या भारतीय यथार्थ को पेश करने वाला साहित्य हो या कस्बे का हो उसे मतलब सुविधा के लिए कुछ लोगों ने कस्बा शहर गांव में बांटा उसकी कोई जरूरत नहीं थी वो एक तरह से बहुत ही जिसे कह चाहिए प्रगड़ भारतीय अनुभव था
डॉ पौराणिक:- जी और यह जो नई कहानी आंदोलन हुआ क्या आप उसको उसके साथ अर्थ मिलाकर देखते हैं या वह नाम देना आप उचित समझते हैं?
कमलेश्वरजी:- मैं समझता हूं कि नाम देने से कोई नुकसान नहीं है खास तौर से इसलिए कि आंदोलन निश्चित रूप से लोगों को ज्यादा सतर्क बनाते हैं पाठक के कई वर्ग होते हैं कुछ है पढ़ते हैं उसको मतलब समझते हैं कुछ है उससे जो चीज लेना चाहते हैं कुछ है कि वो यह देखते हैं कि साहित्य या रचना किस तरह से समाज के बदलते हुए मूल्यों को रेखांकित कर रही है साहित्य किसके साथ खड़ा है किसकी बात करना चाहता है ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि आजादी के तत्काल पहले जो कहानी हमारे पास थी उस कहानी में अगर डॉक्टर साहब आप याद करें तो उस समय एक सवाल पूछा जाता था हम लोगों से जब हम पढ़ रहे थे कि लेखक की फला रचना के माध्यम से यह बताइए कि लेखक का लेखक का जीवन दर्शन क्या है? यानी जो पात्र स्थितियां वो पात्र स्थितियां लेखक क्रिएट करता था इसलिए उसके जीवन दर्शन की तलाश की जाती थी कि वो क्या सोच रहा है जैसे कि अब आप मैं मतलब बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं हमारे अग्रज है ये जयन्य जी है अगेग्य जी है जयन्य जी के साथ यह था कि भाई गांधीवाद किस तरह जुड़ा हुआ है? हे ना या के प्रेमचंद जी के साथ भी आदर्श नमु यथार्थवाद लगाना पड़ा तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लेखक का जीवन दर्शन क्यों तलाश रहे? पात्र तो वो अपने समय से उठा रहा है तो आप अपने समय का जीवन दर्शन की तलाश तो नई कहानी का यह संक्रमण मुझे लगा कि एक महत्त्वपूर्ण संक्रमण था।
डॉ पौराणिक:- और अब इन तीन चार दशकों के बाद पांच दशकों के बाद आपको लगता है कि उस आंदोलन ने या व जो भी समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया थी और जो आपके साहित्य में और आपके समकालीन लेखकों के साहित्य में परिलक्षित हुई वह अपने उद्देश्यों में या अपने लक्ष्यों में कहां तक सफल हुई सार्थक हुई और अब व किस पड़ाव पर आ पहुंची है?
कमलेश्वरजी:- मुझे लगता है कि वह प्रक्रिया एक सोच की प्रक्रिया थी और इसीलिए मैं इस बात को हमेशा मानता था कि नई कहानी कहानी ठीक है अपनी जगह पर है लेकिन नया जब तक निरंतर परिवर्तित नहीं होता वह नया नहीं बना रह सकता तो नये की शर्त यह है कि वो निरंतर परिवर्तित हो और इसलिए मुझे लगता है कि जो पिछले पांच दशकों में या चार दशकों में जो कहानी ने प्रगति की है इतने विराट क्षेत्रों में प्रगति की। इतनी शब्द संपदा पैदा की है इतनी अपनी बोलियों के शब्द लेकर आए भारतीय भाषाओं के शब्द लेके आए या यहां तक के जो जिस का आपने नाम लिया समांतर आंदोलन समांतर खुद मराठी का शब्द है हिंदी में वो है समानांतर हे ना तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाषा जिस तरह से मतलब अपना संस्कार करती है और जब भाषा संस्कार करती है तो निश्चित रूप से भाषा हे ना अपने समय के संवेग और आवेग को लेके आती है और अपने सत्य को स्थापित करना चाहती है
डॉ पौराणिक:- जी हाँ।
कमलेश्वरजी:- और जो रूप मुझे अभी दिखाई पड़ता है मुझे तो लगता है कि बहुत ही यानी सुखद है मेरे लिए तो। जी इतना विकास इतनी तरह की जानकारियां इतनी गहरी प्रतीतिआं।
डॉ पौराणिक:- जी हाँ।
कमलेश्वरजी:- आत्मा की मनुष्य की नियति की मनुष्य के अपने न्याय की आकांक्षाओं की मनुष्य के सपने की
डॉ पौराणिक:- जी हाँ।
कमलेश्वरजी:- अगर कहानी ने यह कर लिया मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
डॉ पौराणिक:- आपके संतोष और आपकी इस आशावादी का मैं कायल हूं खासतौर से जबकि हम प्राय बड़ी निराशा वाली समीक्षाएं या आलोचनाएं सुनते रहते हैं साहित्य की दृष्टि को लेकर भी और और भी बड़े हम वृहत्तर परिपेक्ष में जाए तो हिंदी भाषा और भारतीय भाषाओं की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर बहुत से विचारों को विचारकों को दुख होता है।
कमलेश्वरजी:- जी जी।
डॉ पौराणिक:- कि जिस तरह से अंग्रेजी का एक नव साम्राज्यवादी रूप हमारे ऊपर हावी चला होता जा रहा है और अब इंटरनेट के आगमन के पश्चात तो उसकी पैठ और ज्यादा गहरी हो गई है और इस दबाव को ना केवल हिंदी ने बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं ने एशियाई भाषाओं ने और यहां तक कि यूरोप की अन्य भाषाओं ने भी महसूस किया है तो इस हालात को देखते हुए आप हिंदी भाषा साहित्य और साहित्य से इतर क्षेत्रों में भी उसके भविष्य को किस रूप में देखते हैं और वर्तमान स्थिति को किस रूप में देखते हैं?
कमलेश्वरजी:- मैं समझता हूं डॉक्टर साहब! यह एक बहुत बड़ा चक्रवात आया हुआ है और जब चक्रवात आता है तो निश्चित रूप से कुछ आपकी धरती भी छीन लेता है आपसे कुछ आपके पेड़ों का नुकसान करता है कुछ बस्तियां उजाड़ है कुछ जाने ले लेता है तो यह चक्रवात एक बड़ा जबरदस्त जिसे कहना चाहिए आर्थिक चक्रवात है यह भाषाई चक्रवात नहीं है उतना मूल रूप से ये आर्थिक चक्रवात है और आर्थिक जो मतलब एक ध्रुवीकरण जो दुनिया का हुआ है जिसने कि वैश्विक बाजारवाद की परिभाषा तैयार की है जी उसमें से कहीं ना कहीं एक बात बहुत स्पष्ट होके आती है कि जो भी पूंजी आएगी पहले अर्थ की बात कर ले फिर भाषा पर चले जाए जो भी पूंजी आती है अगर वो पूंजी मनुष्य के पसीने और रक्त से सनी हुई नहीं है तब तो वो कुछ पवित्र पैदा कर सकती है पूंजी की पवित्रता जैसा कि गांधी जी ने कहा था लक्ष्य और साधन।
डॉ पौराणिक:- दोनों महत्वपूर्ण है।
कमलेश्वरजी:- दोनों दोनों महत्वपूर्ण है तो उस रूप में जब पूंजी ही मतलब यानी एक पाप से शोषण से पाप से रक्त से धुली हुई आएगी उसमें सनी हुई आएगी तो पूजी क्या करेगी वो तो रक्त ही चूसेगी हे ना तो इस स्थिति में अब आप भाषा पर आ जाए अब आप भाषा जो उन्होंने भाषा विकसित की है चाहे वो मतलब इंटरनेट की भाषा है या जिस तरह के एविएशंस हुए हैं हे ना मैं आपको बता रहा हूं अभी पांच सात दिन पहले की बात एक आर्थिक अखबार अंग्रेजी का खूब पढ़ा लिखा बच्चा वो पढ़ रहा था 18 साल का था कहने लगे मेरे को समझ में ही नहीं आता इसमें मैंने कहा- क्या हुआ? कहने लगे इसके टर्म्स इतने बदल गए कि अब इन टर्म्स को तब तक जब तक कि मैं कॉमर्स ना पढ़ूं मैं समझ नहीं सकता तो तो अब यह जो भाषा की दिक्कत आई है यह भाषा की दिक्कत हमारे यहां कुछ फैशन के तहत भी आई है जैसे हमारे यहां अभी हिंदी में और तत्काल मतलब जो भी कुछ अंग्रेजी में आया उसको आपने देवनागरी में लिख लिया।
डॉ पौराणिक:- कृत्रिम अनुवाद।
कमलेश्वरजी:- भारती भाषा कृत्रिम वो भारती भाषाओं में भी हो रहा है और ये थोड़ा बहुत होता रहता है इसमें मेरे ख्याल से इससे कोई घबराने की बात नहीं है आप सोचिए कि एक जमाने में खुद दूरदर्शन पर मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा हिंग्लिश आई थी। हिंदी और अंग्रेजी लेकिन आज कहां?
डॉ पौराणिक:- आपको लगता है वो कम हो गई?
कमलेश्वरजी:- उस समय कहां है? आज उनके पास वो भाषा नहीं है आज उन्हें हिंदी में बात करनी पड़ती उसी तरह से आप देखिए कि अपनी दूसरी भाषाओं के जो मतलब चैनल्स आए हैं उनमें भी तब तक जब तक आप अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा की बात अपनी भाषा के माध्यम से नहीं करेंगे तब तक ये कितनी देर की संस्कृति है ये इंग्लिश कितनी देर की या अंग्रेजी मतलब एव्रीवेशन की संस्कृति कितनी देर आप डिस्को में नाचेंगे कितनी देर आप मतलब इंटरनेट के ऊपर बैठ के दूसरे देशों के बारे में और उनकी जानकारियां और ये सब आप इकट्ठी करेंगे हे ना यहां तक के आपके अपने उच्चारण जो अगर आप इंटर इंटरनेट से डाउनलोड करें तो आपके अपने उच्चारण भी आपको दोबारा समझने पड़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है एनीवे मुझे ये लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अब ये प्रिंट मीडिया में भी ये चीजें जा रही अच्छा अब इसको दोनों तरह से देखिए आप एक तो आप इससे यह देखिए कि इसने मतलब हमारी भाषाओं को प्रदूषित किया हिंदी को भी किया भारतीय भाषाओं को भी किया दूसरी तरह से आप यह देखिए कि हमारी भारतीय भाषाओ और हिंदी के बगैर अंग्रेजी का काम नहीं चल रहा दोनों तरह से आप देख सकते।
डॉ पौराणिक:- पर जैसे आपने प्रदूषण शब्द का उपयोग किया एक तरफ कबीर कहते हैं भाषा बहता नीर है संस्कृत को उजल भाषाए तो परिवर्तित होना ही है
कमलेश्वरजी:- जी जी।
डॉ पौराणिक:- तो हम उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित या दुखी क्यों होते हैं? और क्या वाकई में हमें दुखी होना चाहिए? और क्या हमारे दुखी होने से कोई फर्क पड़ता है?
कमलेश्वरजी:- डॉ साहब दुखी मैं तो बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल इसलिए नहीं हूं दुखी सबसे बड़ी चीज है यानी जो हमारे पास कम्युनिकेशन की सुविधाए आई जो टेक्नोलॉजी ने हमें मतलब संचार के जो माध्यम और साधन दिए हम उनका इस्तेमाल करेंगे उस वक्त बड़ी जबरदस्त एक थ्योरी आई थी मार्शल मैक्लुहान कहा करते थे ‘द मशीन इ द मैसेज’ तो उस समय भी बराबर जब काम करता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब भी मैं सोचता था ‘मशीन कैन नेवर बी द मैसेज’, ‘द मैन बिहाइंड द मशीन इज गोइंग टू द मेसेज’ व्यक्ति के बगैर आप कहां काम करते हैं अभी हम और आप बैठे हुए हैं हमारे फ्लोर पर कितने लोग मौजूद हैं कंट्रोल रूम में कितने लोग मौजूद हैं ‘दे आर द मेन बिहाइंड द मशीन’ तब ये हम और आप आमने सामने है। हे ना! तो इस तरह से मतलब कभी-कभी हो जाता हे ना कि चटपटे वाक्य रचना करने के लिए कुछ चीजें आती मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान हो पाएगा बल्कि यह तय है कि मनुष्य अपनी संस्कृति के बगैर नहीं जी सकता और अपनी संस्कृति अपनी भाषा से ही प्राप्त होती है जी।
डॉ पौराणिक:- लेकिन फिर एक और संदेह मेरे मन में उठता है आप ‘सारिका’ जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका से संबध रहे उसे उतनी चाइयों तक पहुंचाया वो एक जमाना था और आज भी हम उसको नोटाल्जिया के रूप में याद करते हैं और भी कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं उस समय थी एक के बाद एक बंद होती चली गई उनके स्थान पर जो नई आई उनको लेकर हमारा मन थोड़ा खिन्न रहता है इस परिदृश्य के बारे में आपकी क्या राय है?
कमलेश्वरजी:- मुझे लगता है कि यह बाजारवाद का एक झोंका जो आया है अपने यहां अब तो संपादकों की जरूरत नहीं रह गई प्रबन्ध संपादक चाहिए तो यह जो एक झोंका आया है उसमें से सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरह की आजादी के संग्राम के बाद हमारे तमाम राष्ट्रीय नेताओं में या हमारे जितने भी सामाजिक नेता थे जिन्होंने परिवर्तन की परिकल्पना की थी चाहे वह सामाजिक परिवर्तन हो चाहे वह मतलब साहित्यिक परिवर्तन हो सांस्कृतिक परिवर्तन हो राजनीतिक हो उन्होंने जिस तरह की परिकल्पना की थी उस उस वक्त यह पत्रिकाएं निश्चित रूप से एक बहुत बड़े परिवर्तन की भूमिका निभा रही थी लेकिन उसके बाद डॉक्टर अपूर्व हुआ यह है कि वो संस्थान जो पत्रिकाएं निकालते थे वो अपने लिए पूंजी से ज्यादा मुनाफा कमाने के परिवर्तन के फेर में पड़ जाने की वजह से उनको लगा कि इनकी जरूरत अब क्या है? कोई जरूरत नहीं और इस तरह धीरे-धीरे तमाम भाषाई पत्रिकाएं खास तौर से हिंदी की जी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं बंद हुई और ये एक बड़ा दुखद अध्याय है हिंदी के क्षेत्र में।
डॉ पौराणिक:- क्या आपको लगता है कि इसी बाजारवाद के चलते शायद कुछ अच्छा भविष्य में हो सके यदि कोई चीज आर्थिक दृष्टि से वायबल हो और साथ ही वह जन अभिरुचि हों का भी वाहक बन सके ऐसा कोई संयोग हो सकता है?
कमलेश्वरजी:- निश्चित। होना पड़ेगा इसे डॉक्टर साहब उसकी वजह यह है कि आप जब शोषण करते हैं यानी मुनाफे के लिए जिसकी वजह से आपने पत्रिकाएं बंद की विज्ञापन कम है या विज्ञापन का उतना रेट नहीं मिलता आपको भाषाई तो मुश्किल यह है कि अभी तक तो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मिडिल ऑर्डर के जो मतलब संस्थान है हे ना जिनसे कि आप ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं उनसे निकाल रहे हैं हे ना लेकिन अंतता आपको पहुंचना है अपने सामान्य जन के पास तो ऐसी स्थिति में मुनाफे की जो स्थितियां है वो मुनाफे की स्थितियां तो एक दिन सैचुरेट होंगी और सैचुरेट होंगी तब आपको लगेगा कि हमने कितना बड़ा नुकसान अपना कर दिया तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की पत्रकारिता इस तरह की पत्रिकाएं और इस तरह के और अन्यथा कोई जरूरी नहीं है कि बड़े संस्थान ही पत्र निकाले हे ना छोटे-छोटे प्रयास होते रह सकते हैं हिंदी की लघु पत्रिकाओं का इतिहास इतना बड़ा इतिहास है मुझे लगता है कि निरंतर बंद होने वाली और निरंतर उसके बाद निकलने वाली पत्रिकाओं ने जो इतिहास लिखा है वो इतिहास बड़ी पत्रिकाओं ने नहीं लिखा।
डॉ पौराणिक:- जी हाँ। वापस एक बार साहित्य की दूसरी विधा की ओर लौटते हुए उपन्यास को लेकर यह माना जाता रहा है कि यह हमारे यहां की साहित्य की पुरानी परंपराओं में नहीं रहा हिंदी की और अन्य भारतीय भाषाओं की या संस्कृत के और पश्चिम से आई हुई विधा है
कमलेश्वरजी:- जी हाँ।
डॉ पौराणिक:- लेकिन पिछले एक-दो दशकों में उपन्यास पर हिंदी में बहुत काम हो रहा है इस स्थिति पर आपके क्या विचार है?
कमलेश्वरजी:- मैं समझता हूं कि यह भी एक बड़ा भारी परिदृश्य ये समय हिंदी में मौजूद है कि हुआ यह है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं मतलब इस नजर से अगर देखूं कि कहां भाषाई और कहां अपने आत्मिक और आंतरिक परिवर्तनों की जो परिकल्पना थी जो सपने थे सपना में शब्द बार-बार इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि आज ये शब्द सुनाई नहीं पड़ता गरीब सुनाई नहीं पड़ती शोषण सुनाई नहीं पड़ता दिखाई पड़ता है हे ना तो इस तरह से हमारे यहां की जो बेसिक आधारभूत जो मतलब सच्चाईयां थी उन आधारभूत सच्चाईयों पर पर्दा डाला गया हमें बताया यह गया कि भारतीय मध्यवर्ग आज इतना यानी आर्थिक रूप से संपन्न है कि फ्रांस और जर्मनी और जापान के मध्यवर्ग को मिलाकर भी उससे ज्यादा बड़ा मध्यवर्ग है हमारा मध्यवर्ग सिंगापुर जाता है तो तमाम अन्य देशों के मध्यवर्ग से ज्यादा खर्चा करता है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो एक ऐश्वर्य की जो परिकल्पना की गई तो ऐश्वर्य तो उस समय भी रहा हमारे यहां जब के मतलब हमारे यहां मनुवादी वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी आखिर कुछ लोगों को तो ऐश्वर्य था ही वो तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तब तक जब तक मनुष्य न्याय से ये चीजें नहीं जुड़ेगी तब तक इन चीजों का कोई अर्थ नहीं और उस रूप में मुझे लगता है कि इस रूप में उपन्यास ने भी ठीक है कहीं कहीं हमारे यहां भी इस तरह की चीजें आती हैं जो कलावादी आते हैं ठीक है कम से कम वो भाषा को शब्दों को तरासते हैं तो हमें और अच्छे शब्द मिल जाते हैं लेकिन वोह कलावादी जो लेखन है वो कलावादी जैसे साहित्यवादी भी आप कह सकते हैं या परंपरावादी भी कह सकते हैं जिसे जब पहले जिसको स्वांता सुखाय कहा जाता था हे ना इस तरह का लेखन आता है उससे भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कम से कम शब्दों की तराश मिलती है कुछ और अच्छे अच्छे मतलब वो निकाल के शब्द ले आते हैं लेकिन आप अपने समय के यथार्थ को ना आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते नकार नहीं सकते और उपन्यास ने उस सत्य को लगातार सामने रखा।
डॉ पौराणिक:- जी हाँ।
कमलेश्वरजी:- जी।
डॉ पौराणिक:- एक उपन्यास आपका जो पिछले दिनों बहु चर्चित रहा ‘कितने पाकिस्तान”
कमलेश्वरजी:- जी।
डॉ पौराणिक:- वो शायद इस बात की ओर इशारा करता है रेखांकित करता है कि मनुष्य या बहुत से समाज अपने पहचान के संकट से ग्रस्त हुआ करते हैं
कमलेश्वरजी:- जी।
डॉ पौराणिक:- अपनी आइडेंटिटी की तलाश में वो तरह-तरह की परिभाषाएं तरह-तरह के आधार ढूंढते रहते हैं जी कहीं यह आधार जातीयता होता है तो कहीं राष्ट्रीयता होता है कहीं धर्म या संप्रदाय या पंथ या भाषा या चमड़ी का रंग तो यह जो प्रवृत्तियां है विघटन कारी की हम अपने आप को और छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर बांट के पहचानने लग रहे हैं बजाय कि हम अपने आप को किसी बड़ी समष्टि के अंदर डुबो कर देखें जी तो यह जो द्वंद है दो प्रकार की विपरीत दिशाओं में जाने वाला इसमें आप किसे ज्यादा स्लाग्य मानते? मैं नहीं जानता आप उसे कोई वैल्यू जजमेंट देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे लेकिन फिर भी आपकी खुद की राय क्या है? और आने वाले समय में आप उसे भविष्य में किस और अग्रसर होता हुआ प्रतीत करते मानते हैं?
कमलेश्वरजी:- देखिए डॉक्टर साहब! यह बात मेरे लिए ‘कितने पाकिस्तान” को लेकर लिखने मैं एक तो कई बार बहुत बार रुकना पड़ा, सोचना पड़ा, पढ़ना पड़ा फिर जाके लोगों से ऐसे ही मिलते जुलते कोई मतलब उपन्यास लिखने के लिए आप कलम पेंसिल लेकर नहीं जाते हैं लोगों से मिलने एक दिमाग में एक कंप्यूटर होता है तो वो सब चलता रहता तो मुझे लगा कि सभ्यताओं में जो लगातार विघटन का और अपनी वर्चस्व का जो एक यानी जिसे दम चलता रहा उस दम की वजह से निश्चित रूप से खुद जिसे आप मानवता कहते हैं मानवता व पूरी नहीं थी बल्कि कुछ लोगों ने अपने को मानवता का पर्याय मान के जिस तरह की स्थितियां पैदा की वो स्थितियां निश्चित रूप से मनुष्य के हित में जाने वाली स्थितियां नहीं थी बहरहाल सभ्यताओं के बाद अब आप इतिहास में आ जाए तो इतिहास कब भी अगर आप देखें तो इतिहास में भी अपने अपने वर्चस्व का यह जो एक एकांतिक विभाजन वाद चल रहा है वह कहीं ना कहीं मनुष्य के संपूर्ण मनुष्य के वो केवल भारत का मनुष्य नहीं सबके विरुद्ध जाता है और ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि जो यानी हमारे यहां तो हर चीज पश्चिम से आती है तो तत्काल थोड़ी स्वीकृत होती है तो मतलब जो याने हंटिंगटन का जो प्रोसेस ऑफ सिविजेशन जो आया यह सिद्धांत और विचार ये मैं समझता हूं कि बहुत ही यानी जिसे कह चाहिए खतरनाक, खतरनाक सिद्धांत इसलिए आया कि उस वक्त जब मनुष्य और पूरा परवादय पूरा पूरब है ना धर्मों की जातियों के वर्णों के हे ना एक न्यायपूर्ण सह अस्तित्व की परिकल्पना के लिए प्रतिबंध दिखाई पड़ता है उस वक्त आप मतलब ये के सभ्यताओं के संघर्ष का सिद्धांत लेके आते हैं नहीं तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि इस उपन्यास और सिर्फ इसी उपन्यास के माध्यम से मैंने ही नहीं मैं समझता हूं कि हिंदी के कुछ बड़े अच्छे लेखको ने इन सवालों को शायद मैंने उसको जरा विस्तार में देखने की कोशिश की है सभ्यताओं और इतिहास के विस्तार में लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जातीयता में देखने की मतलब जो जातीय गिरोह बने छोटे-छोटे गिरोह बने अब वो निकलना चाहते हैं तमाम चीजों को तोड़ के कहीं पर आपको यह नहीं मिलेगा कि कोई पात्र कोई भी बड़ा चरित्र जैसे आप यानी मनमोहन पाठक का उपन्यास ले लीजिए गगन घटा घहरानी मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये नाम कभी लिया नहीं जाएगा क्योंकि लोग पढ़ते नहीं आजकल ये कवि। और खासतौर से लेखक तो पढ़ता ही नहीं तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर आप उसपे से ले ले उसके पात्र कहीं भी अपनी मतलब क्षेत्रीय या जातीयता उसमें सांस लेते लेते अब उनकी सासे घुट रही हे ना तो इसलिए बड़े भारी मानवीय फलक की जरूरत उपन्यास पैदा कर रहा है ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष है आज की सोच का।
डॉ पौराणिक:- लेकिन यदि पहचान की विविधता कम हो गई और हम सब लोग होमोजेनाइज हो गए या एक सम हो गए तो तो हमारा जीवन थोड़ा नीरस नहीं हो जाएगा?
कमलेश्वरजी:- डॉक्टर साहब यह एक रूपता नहीं है यह मुझे लगता है कि यह विविधता का एक दूसरा संस्करण है
डॉ पौराणिक:- जी।
कमलेश्वरजी:- जी। क्योंकि कहीं भी मनुष्य को साहित्य ने बाधित करने की बात नहीं सोची लेकिन मनुष्य सिर्फ मतलब अगर मान लीजिए नदी किनारे बैठा हुआ है नदी किनारे तो 24 घंटे नहीं बैठा रहेगा हे ना या उसे मतलब ये कि बदलती हुई दुनिया एक दौर था जबकि अगर एक इमली का पेड़ या एक आम का पेड़ कट गया व पेट्रोल पंप लग गया हे ना तो नॉस्टैल्जिक इतने हो जाते थे अरे साहब हमारा तो इमली का पेड़ हमारा वो आम का पेड़ नहीं और आप यह देखिए कि अब परिवर्तन की जितनी प्रक्रिया चल रही है उसके साथ-साथ मनुष्य को साहित्य उससे जोड़ता जा रहा है लगातार एक दौर आप याद कीजिए जब टेलीग्राम आता था नहीं तार आया
डॉ पौराणिक:- घबरा जाते थे।
कमलेश्वरजी:- और मोहल्ले में रोना पीटना शुरू हो जाता था उस घर में जिसके घर का तार नहीं फिर वो तार कैसे आपकी जिंदगी का हिस्सा बना साहित्य ने ही तो बनाया हे ना जो मतलब यह कि वो तार जो रेलवे लाइन के किनारे लगे रहते थे जिनके ऊपर चिड़िया बैठी रहती थी तारों पर हे ना और उन तारों के खंभों में कुछ अंगून सुनाई पड़ती थी उसको जब आपने संगीत और लय के साथ जोड़ा जीवन में हे ना जब लकड़ी की जगह खिड़कियां बदली और लोहा आया हम तो लोहे की फौलाद की आवाज को आपने जोड़ा तब जाके बदलती है लोगों की भीतर के संवेग की संवेदना है।
डॉ पौराणिक:- जी परिवर्तन का वाहक है साहित्य।
कमलेश्वरजी:- निश्चित। जी जी जी।
डॉ पौराणिक:- एक और बात वापस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आता हूं आपका संबंध उससे इतना अधिक रहा एक चिंता व्यक्त की जाती रही है कि सूचनाओं की अधिकता हो गई है
कमलेश्वरजी:- जी जी।
डॉ पौराणिक:- एक तरफ तो उन्होंने हमारे लिए समाज के लिए भला किया है कि जो विपन्नता थी हम जानकारी को लेकर उसे दूर किया लेकिन कहीं आज इतना अधिक बहुलता हो गई है सूचनाओं की तो कहीं उसके पीछे सत्य कहीं खो तो नहीं जाता है ऐसा आपको तो नहीं लगता?
कमलेश्वरजी:- नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब! बहुलता तो बहुत है इसमें कोई शक लेकिन बहुलता में रिपीटेशन बहुत है
डॉ पौराणिक:- जी
कमलेश्वरजी:- अधिकांश अगर आप देखें तो वही चीज वही, चीज वही, चीज यानी आप एक अखबार पढ़ लीजिए तो फिर दूसरा अखबार या मतलब एक चैनल देख लीजिए तो फिर दूसरे चैनल की जरूरत नहीं रह जाती एकद स्टोरी कोई एक्सक्लूसिव यहां से निकाल लाये वहां से निकालना लाये वो बात दूसरी तो इस रूप में जो यह सूचना की और जानकारी की बहुलता है मुझे लग रहा है कि यह जितना हमारे यानी इंटीरियर में उन क्षेत्रों में प्रदेशों में पहुंचेगी जहां के इसकी जरूरत है उसको पहुंचने देना चाहिए एक दौर मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खुद याद आता है कि जब हम दूरदर्शन पर यानी ग्रामीण भाइयों के लिए प्रोग्राम ‘चौपाल’ किया करते थे तो हमारे जो मतलब मनोरंजन चाहने वाले दर्शक थे बहुत नाराज होते थे बहुत लेकिन आप देखिए डॉक्टर साहब हरित क्रांति कहां से आई नहीं उस मनोरंजन वाले मध्यवर्ग ने हरित क्रांत पैदा नहीं की नहीं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सूचनाएं तो मनुष्य का अधिकार है और यह सदी ने बताया।
डॉ पौराणिक:- और वो आवश्यकताओं की पूर्ति अभी नहीं हुई।
कमलेश्वरजी:- नहीं हुई
डॉ पौराणिक:- बहुत जरुरत हैं
कमलेश्वरजी:- बहुत जरुरत हैं जहां तक पहुचना चाहिए वहां तक नहीं पहुँच रही
डॉ पौराणिक:- और एक और सवाल शायद मैं अंत में लेना चाहूंगा कि विभिन्न काल में विभिन्न देश में विचारक प्राय इस बात को लेकर चिंतित होते रहते हैं कि मूल्य का बढ़ रहा है
कमलेश्वरजी:- जी
डॉ पौराणिक:- और उनको लगता है कि सिर्फ उन्हीं का काल ऐसा है जबकि मूल्यों का संकट बढ़ा है शायद पहले सब कुछ अच्छा हुआ करता था क्या आपको भी ऐसा लगता है?
कमलेश्वरजी:- देखिए मूल्यों का संकट तो लगातार बना रहता है किसी भी मतलब विकसित होती संक्रमित होती परिवर्तित होती मतलब सोसाइटी में यह मूल्यों का संक्रमण जब बना रहता तो मूल्य हमेशा या विघटित होते हुए खराब होते हुए बड़ी नाराजगी अरे साहब ये तो चौपट हो रहा है ये चौपट हो रहा है, ये चौपट हो रहा है, ऐसा होता है लेकिन उसी में से कुछ इतना रचनात्मक निकलता है मुझसे किसी ने पूछा था एक बार विदेश में कहने लगे कि आपकी जो मतलब नौजवान पीढ़ी है वो तो बिल्कुल एकदम बदल गई और हिंदुस्तानी की कैसे पहचान करें तो मैंने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तानी को अगर सचमुच पहचानना चाहते हैं तो जब वो 28 वर्ष का हो जाए तब उसे पहचानने की कोशिश कीजिए।
डॉ पौराणिक:- 28
कमलेश्वरजी:- 28 हां क्योंकि उससे पहले हमारा अपना पारिवारिक जो संस्थान है वह अपने बच्चों को बड़ी खुली छूट देता है। 28 वर्ष के बाद आपको एक बनता हुआ भारतीय नजर आने लगता है। 28 के आसपास मेरा मतलब केवल 28 नहीं।
डॉ पौराणिक:- जी।
कमलेश्वरजी:- दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है डॉक्टर साहब! कि मूल्यों का यह संकट कोई इतना बड़ा संकट नहीं है ग्लोबलाइजेशन और यह भूमंडलीकरण जिस तरह से आ रहा है इसका अंततः संघर्ष या टकराव कृषि सभ्यताओं से होने वाला है।
डॉ पौराणिक:- जी हाँ।
कमलेश्वरजी:- और हमारी जो यानी लोक संस्कृतियां और लोक पूंजी है हमारे पास वही इसका मुकाबला कर सकती।
डॉ पौराणिक:- वो तो हमारी अक्षण निधि रहेंगे।
कमलेश्वरजी:- जी।
डॉ पौराणिक:- और वही हमारा सबसे बड़ा संबल है
कमलेश्वरजी:- जी।
डॉ पौराणिक:- और आप जैसे चिंतक आप जैसे साहित्यकार यदि इन सरोकारों से समाज को सचेत करते रहे उस पर अपनी आशावादी लेकिन चिंतापूर्णी प्रतिक्रियाओं के द्वारा समाज को आगाह करते रहे और जिस तरह की प्रगति सोच के स्तर पर विचार के स्तर पर लेखन के स्तर पर हमारे हिंदी साहित्य में हो रही है उसे हम और आगे बढ़ावा देते रहे आपके नेतृत्व में आपके समकालीनों के नेतृत्व में आपके शिष्यों के नेतृत्व में यह हमारे लिए एक अच्छी सुखद अनुभूति है और इंदौर दूरदर्शन के स्टूडियो में आकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपको बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद।
हमें आशा है कि हमारे दर्शक इस चर्चा को रोचक पाएंगे विचार उत्तेजक पाएंगे और किन्हीं किन्हीं अर्थों में उपयोगी जरूर पाएंगे।
एक बार पुनः बहुत धन्यवाद।
कमलेश्वरजी:- मैं आपका आभारी हूँ।
***