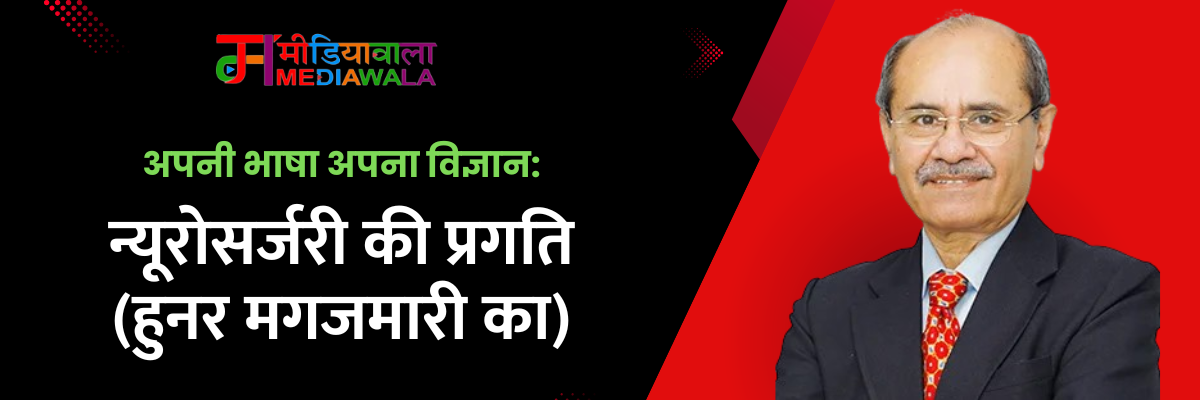आदरणीय मंच और इस प्रशस्थ सभागार में बैठे हुए तमाम सुधी जन,
मैं बहुत खुश हूं कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और विशेषकर उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और इस महान संस्था के कर्णधार, संचालक और इसके समर्पित कार्यकर्ता, इन सबके बीच में आकर मैं बहुत अल्हादित हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
एक विद्यालय के वार्षिक सम्मेलन में भला एक डॉक्टर की क्या भूमिका हो सकती है?
एक बुद्धिजीवी नागरिक के रूप में,
चूंकि मैं खुद एक मेडिकल टीचर रहा हूं, इस रूप में
चूंकि मैं जन स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत मरीजों और आम जनता की शिक्षा करता रहता हूं इस रूप में
और एक पिता और दादा और नाना के रूप में मैं अपने पोते-पोती, नाती-नातियों की शिक्षा में भी योगदान देता हूं। अत: मेरा भी कुछ न कुछ तो योगदान है।
एक छात्र के रूप में मेरी पृष्ठभूमि कुछ भिन्न रही। मैं रतलाम के शासकीय हिंदी माध्यम के टाट पट्टी स्कूलों में पढ़ा। मुझे यहां आकर एक अपनापन लगा। आज जब एक के बाद एक माता-पिता अपनी संतान के साथ पुरस्कार लेने आते जा रहे थे, मुझे उनमें मेरे बचपन की याद आ रही थी। मेरे माता-पिता की याद आ रही थी। सब मध्यमवर्गीय परिवार के सीधे साधे भोले-भाले परिवार थे। उनको देखकर मैं भावुक हो रहा था।
आप सबको बहुत-बहुत बधाई! मैं भला क्या कह सकता हूं? मैं सोच रहा था। लेकिन इसी बीच में मुझे याद आ गया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान व्यक्ति श्री अब्राहम लिंकन का नाम। अब्राहम लिंकन का एक पत्र बड़ा प्रसिद्ध है। आप में से कुछ लोगों ने उसे पढ़ा होगा या उसके बारे में सुना होगा जो उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था। उस पत्र के कुछ अंश मैं उद्धृत करूंगा और उनको वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा।
समय बदल चुका है। अब्राहम लिंकन यदि आज वह पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखते तो शायद उसमें कुछ बातें और जोड़ देते। अब्राहम लिंकन 19वीं शताब्दी के मध्य में थे। मतलब सन 1800 का युग था। अभी परिस्थितियां, डेढ़ सो साल में बदल गई हैं। और फिर यदि वह शिक्षक अब्राहम लिंकन को बदले में पत्र लिखता कि हे पालक, हे पिता, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं, वह भी कुछ बातें मैं अपने इस वक्तव्य में शामिल कर रहा हूं।
अब्राहम लिंकन अपने पत्र में लिखते हैं कि

वे चाहते हैं कि उनका शिक्षक उनके बेटे को सिखाए स्थित प्रज्ञता। जो हम अपने धीरोदत्त नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्मृति कराता है। हीरो के रूप में ऐसा गुण मेरे बच्चे को सिखाना। इसके लिए अब्राहम लिंकन लिखते हैं

ऐसी कई बातें हैं उस पत्र के अंदर। मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि यदि आज के संदर्भ में एक पिता अपने पुत्र के शिक्षक, अपनी पुत्री के शिक्षक के लिए कुछ लिखता तो और भी कुछ बातें कहता।
एक बात जो उन्होंने कही थी वह बड़ी महत्वपूर्ण है:

स्कूल के संदर्भ में इस बात को कहूंगा कि कुछ बच्चों के अंदर दादागिरी की भावना होती है। उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है ‘बुलिंग’। मुझे बुलिंग करने वाले लड़के-लड़कियां बुरे लगते हैं। बेचारे दूसरे बच्चे उनसे डरते हैं। यहां पर वह शिक्षक अपने छात्र के पिताओ से, माताओं से कहेगा कि आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपकी संतान बुली तो नहीं बन रही है। उसको बड़े बाप-पने का अहंकार मत देना। यह आज का शिक्षक पेरेंट से कहना चाहेगा कि ‘आप भले ही कितने बड़े बाप हो, लेकिन अपने बाप का अहंकार अपने बेटे को मत देना। क्योंकि अहंकार ने रावण जैसे बलशाली और विद्वान का भी ध्वंस कर दिया था।

कितना सटीक संतुलन है लिंकन के शब्दों में। हिंसा या आक्रामकता का विरोध है लेकिन “कायर की अंहिंसा” का समर्थन नहीं है।
उसे सिखाना आज के संदर्भ में कि कोई भेदभाव ना करे, कोई स्टीरियो टाइपिंग ना करें। मैंने देखा है स्कूलों के अंदर अनेक बच्चे कुछ भेदभाव या स्टीरियोटाइपिंग या Shaming मतलब शर्मिंदा करना, एक दूसरे को या डिस्क्रिमिनेट करना, या भेदभाव करना बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। यहां पर माता-पिता की जिम्मेदारी आती है कि वो अपने बच्चे में उचित संस्कार डाले।
उसे उचित भाषा सिखाना। यदि माता-पिता या उनके घर के लोग गाली-गलोज करते हैं तो बच्चा भी वही भाषा सीखता है। ये भाषा वो कहां से सीख के आता है? डिस्क्रिमिनेशन के लिए अनेक शब्द है जिनसे हमें बचना चाहिए जैसे मोटू, कालू, लंबू, भिखारी। इस तरह की भाषा हमारे बच्चे ना बोले, एक दूसरे से भेदभाव ना करें। ये शिक्षकों की जिम्मेदारी भी है और माता-पिता की जिम्मेदारी भी है। हमें बच्चों को यह सिखाना है कि जाति, धर्म, नस्ल और भाषा के नाम पर हम कभी भी स्टीरियोटाइप ना करें।
“अरे सरदार तो सब ऐसे ही होते हैं”, “बनिए तो सब कंजूस होते हैं”, “अरे सिंधी तो सब ऐसे ही काईया होते हैं”। इस तरह की बातें हमें नहीं करना है। इस तरह के चुटकुलों को बढ़ावा नहीं देना है। फलां समाज के लोग तो ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग तो ऐसे होते हैं। इस तरह की बातें हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें हमारे बच्चों के द्वारा स्कूल में नहीं होनी चाहिए। यह शिक्षा हमारे माता-पिता की तरफ से हमारे बच्चों को और हमारे शिक्षकों की तरफ से हमारे बच्चों के बीच में आनी चाहिए।
हमारे शिक्षक बच्चों के पालकों से कहना चाहेंगे, उस पत्र में कि आप अपने बच्चे के अंदर यह संस्कार डालें कि वो पैसे के पीछे ना भागे। कब भागेंगे? जब आप खुद भाग रहे हैं। यदि वो रोज देखता है अपने पिता को बात करते हुए कि ‘मेरी इतनी कमाई है, मैंने इतनी ऊंची कार खरीद ली, मैंने यह कर लिया, मैं उससे ज्यादा कमाता हूं, आपका बच्चा भी बचपन से वही संस्कार पाएगा कि मेरे को भी पैसे के पीछे भागना है।
आपको उसको यह दिखाना है कि ‘मेरे को ज्ञान के पीछे भागना है, मेरे को अच्छे गुण के पीछे भागना है।’ यह संस्कार कौन देगा? आप। ठीक है, आप बड़े बाप हो सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है। आपके पास अहंकार आ जाता है। किस तरह का अहंकार? पैसे का अहंकार, पद का अहंकार, या बाहुबल का अहंकार। आप बड़े दादा हैं, गुंडे हैं, आपके साथ बहुत सारी टीम चलती है, गुंडागिर्दी की। बाहुबल का अहंकार, कोई सा भी अहंकार, आपकी संतान को एक अच्छा छात्र नहीं बनने देगा।
उसके अंदर पढ़ने की आदत डालना, लिंकन कहते हैं अपने उस पत्र में,

यह पढ़ने की आदत घर से आनी चाहिए। माता-पिता के लिए यह मैसेज है। अगर लिंकन आज ये पत्र लिख रहे होते तो कहते कि घर में पत्र-पत्रिकाएं होनी चाहिए, घर में किताबों का एक कोना होना चाहिए, घर में किताबों पर चर्चा होनी चाहिए।
मुझे खुशी है कि यहां की लाइब्रेरी इतनी समृद्ध है। मैं चाहूंगा कि यहां के टीचर्स छात्रों के अंदर लाइब्रेरी का उपयोग बढ़ाने की प्रवृत्तियों पर और विचार करें कि कैसे छात्र अपने कोर्स के अलावा अन्य चीजें भी पढ़ें। मैं कल्पना करता हूं कि आज के समय यदि अब्राहम लिंकन एक पत्र लिखते पालक के नाम कि प्रकृति के पास ले जाऊ। मैं माता-पिता से आवाहन करूंगा कि वे खुद जाएं, ट्रैकिंग पर जाएं, घूमने के लिए जाएं, जंगल में जाएं, प्रकृति के पास जाएं, हरियाली में जाएं।
अब्राहम लिंकन के पत्र को लेकर मैं दो लाइन और उद्द᳙त कर रहा हु

मैं जानना चाहूंगा कि कितने माता-पिता अपने बच्चों के साथ कहीं प्राकृतिक भ्रमण पर जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं। नेचर बहुत बड़ी हीलर है।
यह भी मैं चाहूँगा कि स्कूल के माध्यम से बच्चों को बाहर जाने का मौका मिले। कम से कम उस चीज की हम प्रेरणा देंगे। अब्राहम लिंकन अपने शिक्षक को कहते हैं कि

अनेक बातें हैं उस पत्र के अंदर, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं वर्तमान संदर्भ में फिर जोड़ना चाहूंगा। अभी हम को-एजुकेशन की बात कर रहे थे। बहुत सारे स्कूल हैं इंदौर में अन्य शहरों में जहां को-एजुकेशन है। को-एजुकेशन के अपने फायदे हैं, उसकी कुछ चिंताएं भी होती हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन यह युग बदल रहा है। यह संस्कार बदल रहे है।
एक लड़का और लड़की की मित्रता, खासतौर से जब वे किशोरावस्था में आ जाते हैं, जब उनकी प्यूबर्टी आ जाती है, जब उनके हार्मोन निकलने लगते हैं, एक किशोर और किशोरी के बीच में बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है। यह बड़ी सेंसिटिव, बड़ी संवेदनशील, बड़ी नाजुक उम्र होती है। इसको कैसे साधना। इसमें माता-पिता को चिंतन करना पड़ता है और इसमें शिक्षकों को भी ध्यान रखना पड़ता है।
मैं सह शिक्षा का समर्थक हूं। इसके लिए माता-पिता को अपनी बेटा और बेटी को क्या सीख देना है, क्या शिक्षण देना है। यहां पर एक मुद्दा उठता है यौन शिक्षा का। यौन शिक्षा भी अपने आप में एक विवादास्पद विषय है। मैं नहीं जानता कि इस विद्यालय की क्या नीति है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि सेक्स एजुकेशन या यौन शिक्षा क्लास 10, 11, 12 के आसपास धीमी गति से आरंभ होनी चाहिए। उसको बताने का एक संयत तरीका होता है। इस बढ़ती हुई संवेदनशील उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
एक और चीज जो अब्राहम लिंकन के समय नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पत्र में नहीं लिखी, लेकिन दुर्भाग्य से आज के जमाने में बढ़ गई है और वह है नाना प्रकार के नशे। मैं दुखी हो जाता हूं अखबारों में पढ़कर कि हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल के लड़के-लड़कियां शराब पीने लग गए हैं। मैं सिर धुनने लगता हूं अपने आप का।
अगर घर में माता-पिता ड्रिंक कर रहे हैं तो वही चीज बचपन से बच्चों के पास जाएगी। यहां जिम्मेदारी आती है माता-पिता के ऊपर कि वे अपने बच्चों को कैसे संस्कार देंगे। उनके सामने पिएंगे कि अलग से लेंगे या ना लेंगे। दुर्भाग्य हमारी फिल्में शराब को गौरवान्वित करती हैं। हमारे हीरो-हीरोइन ड्रिंक करते हैं। कैसा समाज हमारा होता चला जा रहा है?
यह जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों की, हमारे मैनेजमेंट की, हमारे माता-पिता की है कि कोई बताए कि
“It is not cool thing to drink”
यह कोई स्मार्ट काम नहीं है। इन बातों पर माता-पिता को जोर देना पड़ेगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छी बन पाएंगी।
मुझे बेहद खुशी है कि इस विद्यालय में स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं एक और चीज अपने माता-पिता के लिये कहलवाना चाहूंगा। शिक्षक के द्वारा माता-पिता से उस पत्र में कहलवाउंगा।
शारीरिक परिश्रम हमारी पीढ़ी धीरे-धीरे परिश्रम से दूर हटती जा रही है। हम सुविधाजीवी होते चले जा रहे हैं। एक रिमोट से हम टीवी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं। हम पैदल 100 मीटर भी जाना है तो मोटर बाइक पर या कार में बैठकर जाते हैं। हम घर में सफाई नहीं करते, हमारे यहां हेल्पर लोग आ जाते हैं, काम करने वाले हो जाते हैं। हमें पानी का एक गिलास भी पीना है तो हम बाई को या सर्वेंट को बोलते हैं कि मेरे लिए पानी लाकर दे दे। हम अपना काम स्वयं करना भूलते चले जा रहे हैं।
सारे माता-पिता पर जिम्मेदारी है अपनी संतानों के लिए कि वे उनको परिश्रम का महत्व सिखाएं। घर में सफाई करने का, गली में सफाई करने का महत्व सिखाएं।
दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा प्रणाली में Syllabus या पाठ्यक्रम का आकार बढ़ता ही जाता है।
ढेर सारी किताबें। किताबों की मोटाई। बच्चों पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का बोझा। रटो-रटो-रटो-उगलो-उगलो-उगलो। बस यही पैमाना रह गया है योग्यता का। इस प्रणाली को बदलना किसी एक स्कुल के अधिकार के बाहर है। फिर भी प्रयास होना चाहिये कि रचनात्मक [Creativity] और कल्पनाशीलता [Imagination] को बढ़ावा मिले।
मुझे बहुत खुशी है कि इस स्कूल में बच्चों की क्रियाशीलता का बढ़ावा दिया जाता है। उनकी कल्पनाशीलता, जिसके कि उदाहरण मैंने आज बाहर चारों हाउस के बनाए हुए सुसज्जित प्रेजेंटेशन के अंदर देखे। मुझे बहुत खुशी हुई उसको देखकर।
एक और छोटा सा अनुरोध और है। यह विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। ठीक है, उसको लेकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, मैं उस एजुकेशन पॉलिसी में जो भारतीय भाषाओं में माध्यम बनाने का समर्थन किया है उस नीति का पुरजोर समर्थक हूं। मैं खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा हूं और ठीक है, अंग्रेजी माध्यम है तो है, लेकिन तमाम शिक्षकों से और मैनेजमेंट से और पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की हिंदी और मातृभाषा को बनाए रखने को न भूलें। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
हमारे बच्चे हिंदी भूलते जा रहे हैं उनको अंग्रेजी भी उतनी अच्छी नहीं आती। वे ना घर के, ना घाट के। वे किसी भी भाषा में नहीं। वे अंग्रेजी में अच्छे बने, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन उनकी हिंदी छूटती जा रही है। हिंदी में लिखना-पढ़ना खत्म होता जा रहा है। आप रखो अंग्रेजी माध्यम, लेकिन दैनिक कामकाज में, लेखन में, पढ़ने में उनकी हिंदी अच्छी बनी रहे। मैं चाहूंगा कि यह विद्यालय उसके ऊपर भी ध्यान दे।
मैं यह भी चाहूंगा कि हम अपने बच्चों में थोड़े बहुत संस्कार आध्यात्मिकता के भी डालें। वह शिक्षक की तरफ से भी आना चाहिए और माता-पिता की तरफ से भी। उन्हें स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन से थोड़ा सा परिचय कराएं। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि आंख बंद करके ईश्वर का या जो भी आपके इष्ट देवता हैं, या जो प्रकृति है, उसका ध्यान करने से मन को कितनी शांति मिलती है। कोई मंत्र पढ़ने से मन को कितनी शांति मिलती है। इससे भी हम उन्हें जोड़ के रखें।
हम उन्हें यह भी सिखाएं कि वे अपने राष्ट्र, अपने राष्ट्र के इतिहास, और अपनी संस्कृति पर गौरव करना सीखें। जिसको कि आज मैंने बाहर देखा। हमें बिलीफ होना चाहिए अपने देश के ग्रांड नैरेटिव में। वरना दुर्भाग्य से इस देश में बुद्धिजीवियों का जो जमात पिछले 70 सालों तक हावी रही, उन्होंने तो हमको यही सिखाया कि इस राष्ट्र में तो सब कुछ गंदा ही गंदा था। सब कुछ घृणित था। सब कुछ जाति प्रथा थी और छुआछूत थी और सती प्रथा थी। हमने केवल बुराइयां पढ़ी अपने इतिहास के अंदर। हम अपने राष्ट्र गौरव को नहीं जानते थे।
हमें उसपर गर्व करवाना है अपने बच्चों को। जब वे बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तब वे अपने देश की कमियां भी जानेंगे। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। जानना भी चाहिए हमें अपने देश की कमियां, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में हमें बच्चों में इस विचारधारा को पुख्ता करना है कि वे अपने देश के ग्रांड नैरेटिव पर, महान आख्यान पर गर्व करना सीखें।
और अंत में करूंगा कि हम अपने बच्चों से क्या चाहेंगे? वे कौन सी सीख लेकर निकलेंगे अपने जीवन की? तो चूंकि यह वैष्णव स्कूल है, तो मैं गांधी जी के प्रिय भजन की केवल एक लाइन से मेरी बात को खत्म करूंगा:
“वैष्णव जनतो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे।”
बहुत-बहुत धन्यवाद।
***