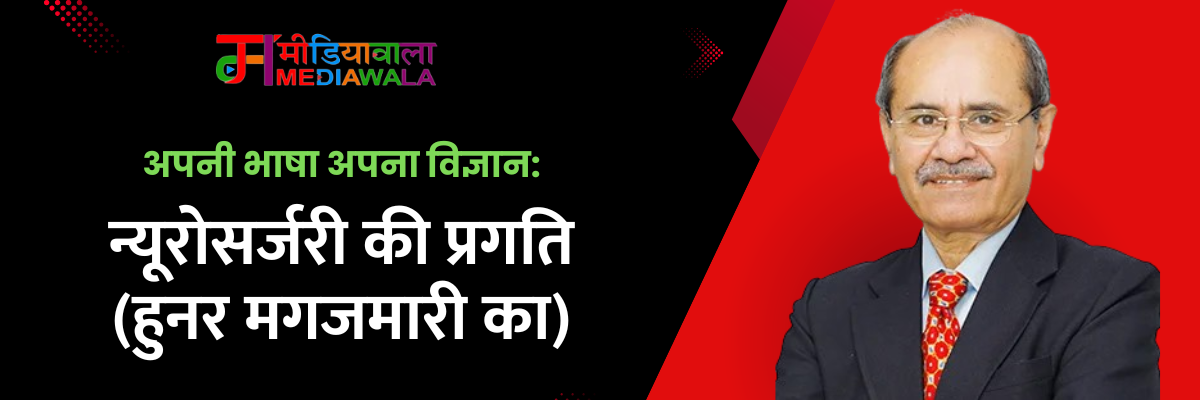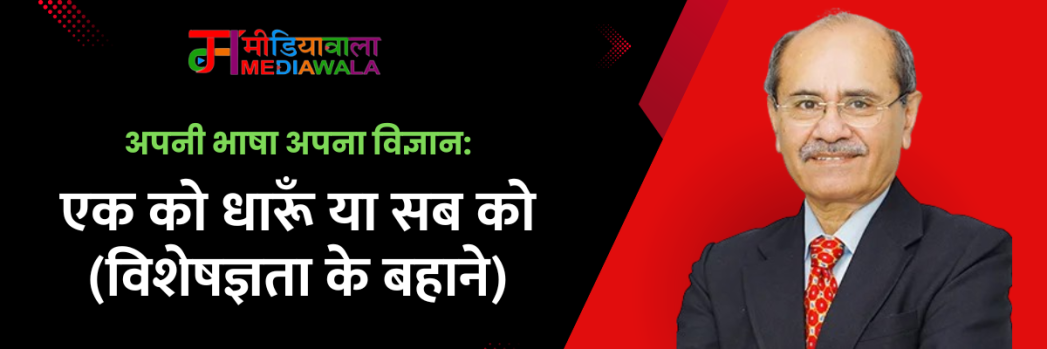
In the year 2000, the department of medicine, M.G.M. Medical College, on the motivation of Dr G.C. Sepaha and under leadership of Dr. P.G. Raman had organised a MILLENNIUM MEET. About 100 past PG students /Residents from last few decades had assembled.
I delivered a debate in twin roles – To be a generalist or to be a specialist?
The resulting essay has undergone a few iterations. Many friends have heard or read it.
I am posting it now as 50th entry for my monthly column at ‘अपनी भाषा अपना विज्ञान’ at online portal MEDIAWALA.
The essay highlights the essence of progress in science or any branch of knowledge and skill to specialization and differentiation ad infinitum. It is an inevitable destiny for mankind. Though many thinkers make futile attempts to castigate it negative terms and to stall it. Yet the march goes on.
एक को धारूँ या सब को (विशेषज्ञता के बहाने)
एक को धारूँ या सब को। कुछ खास बीमारियों का विशेषज्ञ रहूँ या सब की सुधि रखूँ? होऊँ या न होऊँ? To be or not to be एक शाश्वत प्रश्न है। पुरानी दुविधा है। हर युग में नए रूप धरकर आती है। विशेषज्ञ होने के नाते या यूँ कहूँ ज्ञान के एक सीमित क्षेत्र में अधिकाधिक सीखने की अंदरूनी ललक के कारण यह प्रश्न सदैव मेरे सम्मुख प्रस्तुत रहा है। मेरे अकेले का प्रश्न नहीं है। मुझ जैसे अनेक है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन एक सामान्य फिजीशियन भी हूँ तथा एक आम डॉक्टर भी हूँ। मैं क्या हूँ? या फिर मैं मिर्गी रोग विशेषज्ञ या लकवा रोग विशेषज्ञ मात्र हूँ। मेरी अनेक भूमिकाएं हैं। प्रिय कौन सी है? श्रेष्ठतम कौन सी है? समाज के लिए सबसे उपयोगी कौन सी है? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जनता मुझसे क्या अपेक्षा करें? मेरी शिक्षा, योग्यता व संभावनाओं से संस्था व समाज को अधिकतम लाभ कैसे मिल सकता है? ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। यह वृहत्तर महत्व के प्रश्न है जो मुझ जैसे अनेक विशेषज्ञों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है।

एक चुटकुला प्रचलित है। आँख का इलाज करवाने गए मरीज को डॉक्टर ने कहा “मैं सिर्फ दाईं आँख का इलाज करना जानता हूँ। तुम्हारी बाईं आँख खराब है। उसका डॉक्टर दो घर आगे रहता है। “जैसा कि आमतौर पर होता है इस चुटकुले में निहित भावना, अर्ध्य सत्य हैं। पूरा सत्य क्या है? हरफनमौला बने रहे या घर व घाट में से किसी एक के होकर रह जाएँ? मैं व्यक्तिगत तौर पर एक खास विषय का जानकार रहना पसंद करता हूँ बजाये कि ऑलराउंडर बनने के। कौन-सी शैली बेहतर है? जीवन की विधाओं के प्रति समग्र दृष्टि रखें या एकपक्षीय? अतिविशिष्ट, योग्यता चुनें या बहुमुखी योग्यता? क्या दोनों चुनना संभव है?
हमने पुरानी पीढ़ी के फिजिशियन चिकित्सकों को शुरू से आदर की दृष्टि से देखा है। हम पुराने प्राध्यापकों की सर्वतोमुखी प्रतिभा के कायल रहे हैं। उस पीढ़ी के धीरे-धीरे समाप्त होते जाने पर आज हम आँसू बहाते हैं। क्या यह सत्य ही इतने दु:ख का विषय है? हमारी पुरानी पीढ़ी ने भी ऐसा ही शोक व्यक्त किया था जब की पिछली पीढ़ी लुप्त होने लगी थी जो एक साथ फिजीशियन, सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ सबकुछ थी। डॉक्टर एस. के. मुखर्जी गवाह थे आम से खास तक के इस सफर के क्योंकि आरंभिक वर्षों में उन्होंने प्रसव कार्य संपन्न कराए थे और बाद में ह्रदय रोग विज्ञान के कोनों में झाँक कर देखा था।
पुराने यूनान में अरस्तु एक कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, भौतिक शास्त्री, ताराविद सब था, ऑल इन वन। उन दिनों ज्ञान सीमित था। अब हमें अगणित वर्ण बनाना होंगे। और कोई चारा नहीं। हम चाहें या ना चाहें, परिवर्तन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं। सूचना का सतत विस्फोट रूक नहीं सकता। वह फैलता रहेगा। सभ्यता के उषाकाल से मानव मन ने, अपने स्वभाव के अनुरूप, अज्ञान के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा खोल रखा है। समय के साथ यह मोर्चा आकार में बड़ा होता जा रहा है। अधिक सैनिकों की जरूरत है। इसका अर्थ यह नहीं कि आम जानकारी रखने वाले ज्ञानी लोगों की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसका स्वरूप व मात्रा बदल जाएँगे।

परिवर्तन और प्रगति से चौंक कर, हर युग में विचारकों के मुँह से चेतावनी फूट पड़ी है ‘बहुत हो चुका बस करो’। ‘सभ्यता नष्ट हो जाएगी’। ‘प्रलय आ जाएगा’। दुर्दिन की भविष्यवाणियाँ कब नहीं की गई —- आग का उपयोग सीखा, धरती का सीना फाड़ कर हल जोतना और बीज बोना शुरू किया, लिखने पढ़ने का आविष्कार कर ज्ञान को पुस्तक रूप दिया, औद्योगिक क्रांति आई, परमाणु शक्ति का दोहन किया, चिकित्सा द्वारा मृत्यु को कुछ वर्ष टालने की भी कोशिश करी जा रही है, वंशगति वाले जींस को नियंत्रित करने की संभावनाएँ जगाईं गई हैं। कुछ लोगों के मन में हर समय जड़त्व और भय की संभावना भर आती है। परंतु कोई मसीहा या देवदूत कालचक्र की गति को रोक नहीं पाता।
ज्ञान की विभिन्न विधाएँ बार-बार संक्रमण काल से गुजरती हैं। बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में ज्ञान का दायरा सबसे तेजी से फैला है। सूचना का विस्फोट है। किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह अपने सीमित से विषय में हो रहे समस्त परिवर्तन और खोजों की जानकारी रख सके।
एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि सामान्य चिकित्सक व विशेषज्ञ की सोच, प्रकृति, प्रवृत्ति आदि में अनेक अंतर आ जाते हैं।
ज्ञान के आधार में बृहद भेद होता है।
बीमारियों के प्रति नजरिया बदल जाता है। सामान्य चिकित्सक बीमारियों का निदान करते समय उनके आम स्वरूप को ख्याल में रखता है लेकिन अनेक मौकों पर रोगों के लक्षण चिह्न, पाठ्य पुस्तक में दिए गए वर्णन से अलग प्रकार के होते हैं। विशेषज्ञ को इन इतर-रूपों का अधिक अनुभव व ज्ञान होता है। सामान्य चिकित्सक मामूली कारणों से इस रोग का निदान चूक जाते हैं या करने से झिझकते हैं। यदि उसके लक्षण टिपिकल यानी ठेठ किस्म के न हों। उपचार की आधुनिक विधियों का उनका ज्ञान सीमित होता है। मरीज की तासीर और बीमारी के हालात अनुसार औषधि के उपयोग में महीन फर्क करना उन्हें कम आता है। अगर कोई सामान्य चिकित्सक किन्ही बीमारियों का निदान व उपचार श्रेष्ठतम तरीके से करता हो तो यकीनन वह व्यक्तिगत रुचि या अनुभव द्वारा बीमारियों का विशेषज्ञ पहले ही बन चुका होगा। बात डिग्री की नहीं है। बात रुचि व समझ की है। जितना देंगे, उतना पाएँगे। उतने ही विशेषज्ञ बनते जाएंगे। कुछ खोना जरूर पड़ेगा। हर विषय में एक जैसी महारत हासिल करना संभव नहीं।
विशेषज्ञ की रुचियाँ और क्षमताएँ, उसके क्षेत्र के बाहर सामान्यप्रायः समाप्त हो जाती हैं। कहने को कह लो कि आम लोगों की आम तकलीफों के लिए वह काम का आदमी नहीं रह जाता है। लेकिन उसमें अन्य खूबियाँ विकास पा जाती हैं। उच्च अध्ययन के लंबे वर्षों के दौरान उसे ढ़ेर सारी पुस्तकें व शोध पत्रिकाएं पढ़नी होती है, लिखना होता हैं, शोध कार्य करना होता है, विभिन्न मुद्दों की तह में जाकर तफसील से बहस करना होती है, व्याख्या करना सीखता है, विश्लेषण करना सीखता है। जटिल समस्याओं को समझ पाने, बूझ पाने की क्षमता बढ़ती है। अपने आपको एक सीमित क्षेत्र में झोंक देने के बावजूद, जीवन के प्रति पूर्णता या सर्वांगता का बोध गुम नहीं जाता। बल्कि वह तो और ज्यादा विकसित हो जाता है। अंतर का ज्ञान मुक्तिदायक है। कैसा भी ज्ञान हो। शुद्ध, सात्विक, स्वान्त सुखाय ज्ञान। ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए। ज्ञान की खोज में पतली से पतली गली में घुसते चले जाओ वह आपको अंततः विद्या बुद्धि के बृहत्तम क्षितिज तक पहुँचाएगी। किसी भी विषय की गहराइयों में उतरना तथा उसके विकास के सबसे अग्रिम मोर्चे पर रहना, मानसिक दृष्टि से अत्यंत संतोषकारी होगा। जिसने इस आनंद की अनुभूति की, मानों ईश्वर का एहसास कर लिया। शायद इसे ही गीता में तथा बाद में विवेकानंद ने ‘ज्ञान-योग’ के रूप में समझाया।

प्रसिद्ध खगोल शास्त्री व विज्ञान लेखक श्री कार्ल सेगन ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक “स्वर्ग के नाग दैत्य”(“ड्रैगन्स ऑफ़ ईडन”) में कहा है कि छिपकलियों के विकास स्तर तक, मस्तिष्क क्षुद्र था तथा उसमें निहित जानकारी से कहीं अधिक सूचनाएं गुणसूत्रों पर, डीएनए रचना वाली जींस द्वारा नियंत्रित होती थीं। उत्तरोत्तर विकास से मस्तिष्क का आधिपत्य बढ़ता गया। जब से मानव मस्तिष्क ने अपनी अभूतपूर्व क्षमताओं को पाया है, ज्ञान दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इतना अधिक कि स्वयं मस्तिष्क की संग्रहण सीमाओं से अधिक। सूचना विस्फोट के भस्मासुर से निपटने के लिए मनुष्य की मेधा ने फिर नायाब तरकीबें ईज़ाद कर डाली। पहली बार ज्ञान को शरीर मस्तिष्क से बाहर शब्द रूप में लिख कर रखा जाने लगा। पुस्तकों व ग्रंथों के रूप में। और अब कंप्यूटर आ गए हैं जो न केवल अकूत जानकारी भरे रख सकते हैं, वरन उसका विश्लेषण कर समस्याओं का हल, सुझाव दें हैं। सचमुच सोचते हैं। गूगल और ए.आई. आना सांस्कृतिक क्रान्ति के नये उदाहरण है। आगे भी आयेंगे।
क्या ज्ञान सचमुच इतना अच्छा है? क्या ज्ञान सदैव शुद्ध व निर्मल रहता है? क्या ‘अतिसर्वत्र वर्जयेत’ का सूत्र वाक्य ज्ञान पर लागू नहीं होता? कहीं ज्ञान की अधिकता सहज बुद्धि या कॉमन सेंस का हनन तो नहीं करती? मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता। यदि यह संदेह मेरे मन में उठते भी हो तो फिलहाल में उन्हें चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता।
विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास कैसे हो पाया?
बहुत से दीवाने लोगों ने अपनी अपनी प्रज्ञा शक्ति व समय का दान किया। मन की शक्ति ही सब कुछ है। यहां तक कि खेलकूद, संगीत, ललित कला आदि के विकास के मूल में खपने वाली ऊर्जा भी अंतत: मानसिक प्रज्ञाशक्ति हैं। विशेषज्ञों की शोध के बिना विषयों की उन्नति कभी न हो पाती। वे केवल सड़ते रहते, जंग खाते । सौभाग्य से परिदृश्य स्वत: बदलता जाता है। ज्ञान को तो बढ़ना ही है। यह ध्रुव सत्य है। अटल सत्य है। मृत्यु और जन्म के समान। इस ब्रह्मांड की गति के समान। इस कार्य में कुछ लोगों को निमित्त बनना पड़ता है। सब लोग सारे काम पूरी खूबी से नहीं कर सकते। आधे-अधूरे हैं। साथ ही खासम-खास भी है। किसी का योगदान अधिक है। किसी का कम।
प्रसिद्ध खगोल शास्त्री स्टीफेन हॉकिंग व फ्रेड होयेल के अनुसार ब्रह्मांड हर पल, सतत फैलता जा रहा है। एक बड़े गुब्बारे के समान। ज्ञान का गुब्बारा ऐसा ही है। उसे खोजने का अभियान एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ने के समान है जो उलटा रखा है। शिखर नीचे, आधार ऊपर। नीचे पड़ा शिखर अज्ञान का घोतक है, ऊपर फैलता आधार ज्ञान का प्रतीक। ऊपर कोई शिखर नहीं है। जितना चढ़ोगे, अभियान का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता जाएगा । आपको अपने लिए एक छोटा कोना या संकरा मार्ग चुनना पड़ेगा। सबके अपने अपने शिखर।
समाज को सब तरह के लोगों की जरूरत है। अलग-अलग क्षमता व योग्यता वाले लोग। सर्वव्यापी ज्ञान वाले लोगों का भी महत्व है। लेकिन लियोनार्दा विंसी जैसे जीनियस कम होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ था। शिकारी, खेती करने वाला, मकान बनाने वाला, खाना पकाने वाला । सभ्यताओं की बढ़ती जटिलता के साथ कार्य विभाजन की संख्या बढ़ती गई। कम विकसित समाजों में आज भी पुरानी व्यवस्थाएँ देखी जाती है। सभ्यताओं में परिवर्तन की चाल से उनके खुद के विचारक नेता अचंभित रह जाते हैं। प्रत्येक समाज अपना संतुलन ढूँढ लेता है। तेज चलूँ या धीमा चलूँ। किस क्षेत्र में तेज चलूँ तो किस में धीमा।
अनेक प्रशासक भी जड़त्व की भावना से ग्रस्त होते हैं। वे या तो परिवर्तनों से कतराते हैं, या परिवर्तन और विकास चाहने वालों के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। दुर्भाग्य से चिकित्सा विशेषज्ञों के बारे में अनेक गलतफहमियाँ व्याप्त है। कुछ लोगों को लगता है कि ऊँची डिग्री, लंबा प्रशिक्षण, शोध कार्य आदि सब छल है तथा उसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है। यह सत्य नहीं है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के युग में विशेषज्ञ सफल हो पाते हैं यह इस बात की द्योतक है कि समाज में उनकी आवश्यकता है। बाहरी बैसाखियों के बूते पर कोई भी आर्थिक गतिविधि पनप नहीं सकती। उसे अंदर से सक्षम होना होता है। चिकित्सा व्यवसाय का बदलता परिदृश्य जिसमें विशेषज्ञ अधिकाधिक भूमिका निभा रहे हैं, स्वतंत्र उद्यम के नियमों पर आधारित है तथा होना भी चाहिए। जीवन के सबसे बेशकीमती 15 वर्ष झोंक देने के बाद कोई चिकित्सा विशेषज्ञ अपने विषय की प्रथम पंक्ति में प्रवेश ले पाता है। आर्थिक सफलता तब जीवन के अनेक प्रमुख लक्ष्यों में से एक होती है परंतु एक मात्र लक्ष्य नहीं। ज्ञान का दीपक जलाए रखने की अंदरूनी ललक मरती नहीं, मरना भी नहीं चाहिए। वही ललक है जो इंसान को इस मुकाम तक लाती है। पैसा उसका परिणाम है, मुख्य साधन नहीं है।
भारत में, विशेषज्ञ बने या ना बने की दुविधा कहीं ज्यादा ही मुँह बाएँ खड़ी नजर आती है। हमारे यहां घोर गरीबी है। समाज के बड़े तबके की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। फिर भी हम आगे की ओर देखने तथा बढ़ने की कोशिशें त्याग नहीं देते। हम परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित करते हैं, अंतरिक्ष उपग्रह कार्यक्रम चलाते हैं, राष्ट्रीय संस्थान और प्रयोगशालाऐं विकसित करते हैं। आजादी के बाद, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की भविष्य पर दूरदृष्टि ना रही होती तो हम और भी पीछे रह जाते ।
यह पूछने की बजाए कि ‘क्या हम विशेषज्ञ विभागों का खर्चा उठा सकते हैं?’ पूछा जाना चाहिए कि ‘क्या हम सदैव पिछलग्गू बने रहना चाहते हैं’।
न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे मस्तिष्क की उपमा याद आती है जो समानांतर प्रणाली पर काम करता है ना कि श्रेणीगत प्रणाली पर। सूचना का सतत प्रवाह एक साथ ढ़ेर सारे परिपथ में होता रहता है। एक काम निपट जाएगा, फिर दूसरा करेंगे वाली नीति नहीं अपनाता। एक साथ बहुत सारे मोर्चा खोले रहता है। यदि हम सदैव आधारभूत आवश्यकताओं को लेकर रोते रहे तो एक ही स्थान पर कदमताल करते रह जाएंगे। सब लोगों की सब जरूरतें पूरी करने की तानाशाही कोशिश में विचारधाराओं का पतन हो गया। स्वतंत्र उद्यम के आधार पर नए नए क्षेत्रों में विकास होने से पूरा लावजमा आगे खिसकता है और पीछे पीछे प्राथमिक जरूरतों की पूर्ति में मदद करता है।
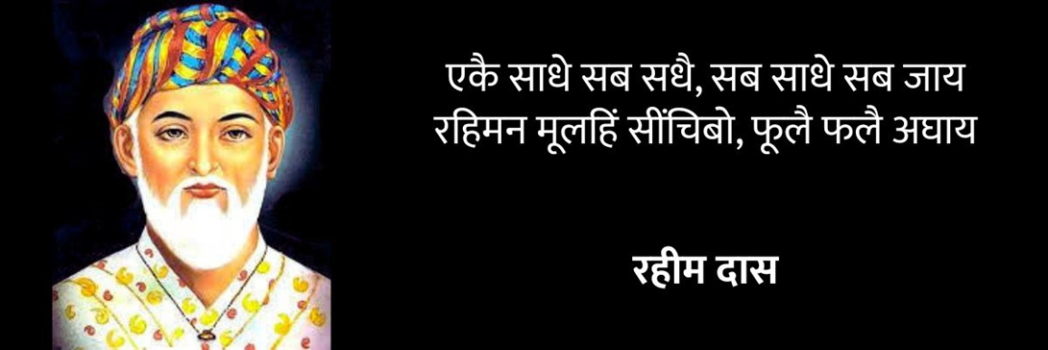
रहीम ने उपरोक्त दोहा एक वृहत्तर दार्शिनिक सन्दर्भ में कहा होगा। लेकिन उनकी पहली पंक्ति मेरे विचार का समर्थन करती है। रहीम किस मूल को सींचने की बात कर रहे है? भक्ति योग वालों के लिये वह ईश्वर या इष्ट देवता हो सकते है।
लेकिन मुझ जैसे ज्ञान वालों के लिये उसका अर्थ है Scientific Temper, Scientific Methods, मीयंसा, खोज-प्रवृत्ति। अपने अपने प्रिय इष्ट-विषय में नवीन ज्ञान का सृजन करते चलो। उसके Applications (तक्नालाजी के आनुशंषिक लाभ) के द्वारा सब कुछ होगा “फूलै फलै अघाय”, यही तो होता रहा है आनादि काल से।
***